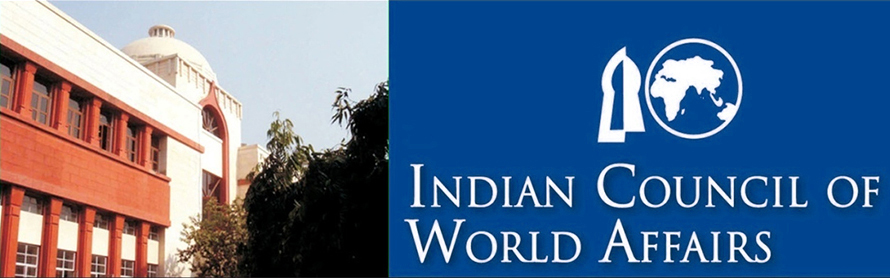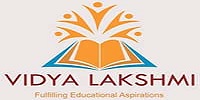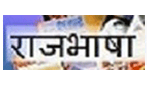भारतीय वैश्विक परिषद
सप्रू हाउस, नई दिल्लीएक्ट ईस्ट पॉलिसी के दस वर्ष होने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मे सुश्री नूतन कपूर महावर, एएस, आईसीडब्ल्यूए द्वारा उद्घाटन भाषण, 24 फरवरी 2025
डॉ. फादर जोसेफ सी.सी., कुलपति, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी,
मलेशिया, चेन्नई के महावाणिज्यदूत - आसियान और एडीएमएम के अध्यक्ष
छात्रों और मित्रों,
मुझे भारतीय वैश्विक परिषद के करीबी समझौता ज्ञापन भागीदारों क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बैंगलोर और चेन्नई सेंटर फॉर चाइना स्टडीज (सी3एस) के द्वारा आयोजित 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी का दशक: भारत-आसियान संबंधों और क्षेत्रीय गतिशीलता पर प्रभाव' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए खुशी हो रही है। मैं उन्हें भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के दस साल पूरे होने के अवसर पर इस पहल के लिए बधाई देता हूं, जो भारत के विदेश नीति लक्ष्यों और उद्देश्यों का प्रमुख स्तंभ है और इसका जायजा लेने और आगे की राह तैयार करने का एक तरीका है।
परिचय
भारत ने 1991 में दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंध बनाने के लिए मुख्य रूप से एक आर्थिक कूटनीति उपकरण के रूप में, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के पहले लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की थी। 90 का दशक का वह दौर था जब रूस की क्रांतिकारी सेना के पतन के बाद दुनिया के कई हिस्सों में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। भारत ने भी 1991 के संकट के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए विस्तृत आर्थिक शोधना की शुरुआत की। कई दक्षिण पूर्व एशियाई देश जिन्होंने अब तक नाटकीय आर्थिक विकास देखा था, लेकिन 90 के दशक के काल में गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। यह 90 के दशक की आर्थिक अशांति थी जिसने लुक ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से भारत और आसियान क्षेत्रो के बीच नए सिरे से संबंधों के लिए पृष्ठभूमि प्रदान की। 90 के दशक में भारत ने क्षेत्रीय संवाद साझेदार से आसियान के पूर्ण संवाद साझेदार के रूप में परिवर्तन देखा, 2002 में भारत-आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत के साथ, जिसने संवाद संबंधों को चालू करने का प्रयास किया।
2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सत्ता में आए, तो उन्होंने महसूस किया कि भारत को क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की अपनी आकांक्षाओं के साथ-साथ अपनी बढ़ती आर्थिक ताकत के अनुरूप दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और उससे आगे के सभी क्षेत्रों में सहयोग के लिए और ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है, इसलिए वे फिर से “एक्ट ईस्ट” पॉलिसी लाए।
लुक ईस्ट पॉलिसी की तुलना में एक्ट ईस्ट पॉलिसी अधिक क्रियाशील है, जिसमें संस्कृति, राजनीति, सुरक्षा और रक्षा, समुद्री और अंतरिक्ष सहित सहयोग के विस्तारित क्षेत्र शामिल हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने दक्षिण-पूर्व एशिया से भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार करके पूर्वी एशिया, पूर्वोत्तर एशिया, ओशिनिया और इंडो-पैसिफिक को व्यापक रूप से शामिल करके “ईस्ट” के अर्थ को भी फिर से परिभाषित किया। हालाँकि, दक्षिण-पूर्व एशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए “केंद्र” बना हुआ है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का आसियान द्वारा स्वागत किया गया है क्योंकि यह आसियान के निर्माण के प्रयासों को पूरा करता है।
शांति, सुरक्षा, स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने के लिए साझा की गई उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आसियान और ‘पूर्व’ के देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना एक्ट ईस्ट पॉलिसी का व्यापक उद्देश्य है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के उद्देश्य आसियान की केंद्रीयता को दोहराते हुए क्षेत्र में सभी भारत-आसियान संबंधों और द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संबंधों के साथ तालमेल और सुसंगत स्थापित करते हैं।
आसियान केंद्रीयता का मतलब है कि आसियान देशों के एकमत निर्णय उनके क्षेत्र से संबंधित मामलों में मान्य होंगे और यह आसियान क्षेत्र के उनके बाहरी भागीदारों को स्वीकार्य होगा। आशा है कि ऐसे एकमत निर्णय लेने में आसियान देश संवाद के माध्यम से क्षेत्र में वैध हितों वाले अन्य देशों के विचारों और चिंताओं को ध्यान में रखेंगे। आसियान केंद्रीयता का महत्व आसियान की आंतरिक दुविधा से उपजा है, जो इस क्षेत्र में महाशक्तियों के बीच रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता और पास और दूर के विदेशों से आसियान के भागीदारों की बहुलता के कारण है। भारत आसियान केंद्रीयता का समर्थक है। भारत आसियान एकता का भी समर्थक है जो राजनीति, अर्थव्यवस्था और बाहरी संबंधों में आसियान के विभिन्न देशों के अलग-अलग नीतियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
एक्ट ईस्ट पॉलिसी की उपलब्धियां
1. भारत- आसियान राजनीतिक सहयोग:
भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने अपनी शुरुआत से ही महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। भारत-आसियान राजनीतिक संबंधों ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो 2022 में उनके संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) के द्वारा उच्चे स्तर पर ले जाएगा और वो उनके साझेदारी के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाने का साल होगा। यह 1991 में शुरू हुए निरंतर लंबे संबंधों का परिणाम था और यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और 2019 के इंडो-पैसिफिक (एओआईपी) पर आसियान के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
2019 का इंडो-पैसिफिक पर आसियान आउटलुक भारत के इंडो-पैसिफिक विजन के साथ तालमेल रखता है और चार प्रमुख क्षेत्रों में मौजूदा आसियान के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय व्यवस्था के माध्यम से भारत-आसियान के सहयोग को बढ़ावा देने में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है, अर्थात समुद्री सहयोग, कनेक्टिविटी, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2030, और आर्थिक सहयोग और क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास में योगदान देने के लिए आगे के सहयोग का आधार प्रदान करता है।
2024 में लाओ पीडीआर में आयोजित पिछले भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान एकता, आसियान केंद्रीयता और इंडो-पैसिफिक पर आसियान दृष्टिकोण के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने भारत-आसियान संबंधों को और मजबूत करने के लिए 10-सूत्रीय योजना की घोषणा की, जिसमें कनेक्टिविटी, व्यापार, डिजिटल परिवर्तन, जलवायु कार्रवाई और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया।
2. भारत-आसियान रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग
आसियान देशों के साथ भारत की रक्षा और सुरक्षा सहयोग इस क्षेत्र में आधुनिक और आगे बढ़ने की विशेष योजना को दिखाता है। आसियान की सुरक्षा चुनौतियों के लिए भारत की प्रतिक्रिया आपसी समझ पर आधारित है, जिसमें सहयोग, क्षमता निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के पालन पर जोर दिया गया है। विश्वास को बढ़ावा देने और आसियान की प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाने के ज़रिए, भारत इस क्षेत्र की उभरती सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने में विश्वसनीय भागीदार है, साथ ही एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को मज़बूती प्रदान करता है, जिसे भारत की 2019 की इंडो-पैसिफिक पहल के सिद्धांतों के रूप में शामिल किया गया है।
i. भू-राजनीतिक और क्षेत्रीय आयाम
आसियान के सामने एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती दक्षिण चीन सागर (एससीएस) पर चीन की "नाइन-डैश लाइन" को लेकर प्रतिस्पर्धी दावे हैं, जो वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई के क्षेत्रीय जल के साथ ओवरलैप होती है। चीन के द्वारा विवादित द्वीपों के सैन्य ने तनाव और टकराव के जोखिम को बढ़ा दिया है। इस तरह के क्षेत्रीय तनाव ने विवादित एससीएस क्षेत्र में भारत के व्यापारिक नौवहन के मार्ग को जोखिम में डाल दिया है। क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, विशेष रूप से एससीएस, यूएनसीएलओएस 1982 के तहत समुद्री अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों को मजबूत करने में भारत की सुरक्षा चिंता रही है। भारत और आसियान दक्षिण चीन सागर (डीओसी) में पार्टियों के आचरण पर घोषणा के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन का भी समर्थन कर रहे हैं।
भारत के क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर) समुद्री दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, भारत आसियान नौसेना बलों के साथ क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और संयुक्त अभ्यासों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, जैसे कि सिंगापुर के साथ 1994 से हर दो साल में एक बार संयुक्त अभ्यास आयोजित किया जाता है। अंतिम अभ्यास 2023 में और एक अभ्यास 7 आसियान देशों यानी ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के साथ 2023 में दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया, वियतनाम के साथ 5वां सेना अभ्यास 2024 में भारत के अंबाला और चंडीमंदिर में आयोजित किया गया और 9वां भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। इसके अलावा, भारत का सिंगापुर के साथ 2017 का द्विपक्षीय समझौता है, जिसके तहत भारतीय नौसेना के जहाजों को चांगी नौसेना बेस पर ईंधन भरने सहित सीमित रसद सहायता की अनुमति है। और, ज़ाहिर है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम और अन्य सहित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में नियमित रूप से बंदरगाहों पर यात्राएं होती रही हैं। भारत इस क्षेत्र के देशों को अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है, जिसमें फिलीपींस को संयुक्त भारत-रूस क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की आपूर्ति भी शामिल है।
भारत आसियान के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में भी सहयोग कर रहा है, जिसमें वियतनाम और इंडोनेशिया में ट्रैकिंग, डेटा रिसेप्शन और प्रोसेसिंग स्टेशन स्थापित करना शामिल है। भारत और ब्रुनेई ने 2024 में पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा के दौरान अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत करने पर भी सहमति जताई।
ii. गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरे
पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के अतिरिक्त, गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत सहयोग का क्षेत्र बनती जा रही हैं।
भारत मानवीय संकटों और प्राकृतिक आपदाओं में अपने सहयोगियों को सहायता भेजने वाला ‘पहला प्रतिक्रिया दाता’ है, उदाहरण के लिए, सितंबर 2024 में चक्रवात यागी से प्रभावित आसियान देशों को ‘ऑपरेशन सद्भाव’ चलाया गया। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत एक और उपलब्धि भारत की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत आसियान देशों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति है।
आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम) के रूपरेखा में और साथ में दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महिलाओं के लिए पहल और समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण प्रतिक्रिया पहल जैसी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। भारत और इंडोनेशिया ने 2020-2023 के लिए एचएडीआर पर एडीएमएम+ विशेषज्ञ कार्य समूह की सह-अध्यक्षता की।
इसके अलावा, एडीएमएम+ के तहत, आसियान देशों में साइबर खतरों से निपटने के लिए कई संवाद और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जो कई आसियान देशों में सीमित साइबर सुरक्षा संरचना और विशेषज्ञता का सामना करते हैं। भारत इस कमी को पूरा कर सकता है।
भारत ने 2024 में आतंकवाद-रोधी एडीएमएम+ विशेषज्ञ कार्य समूह में भी भाग लिया, जिसमें आतंकवाद में ड्रोन और एआई के उपयोग जैसे उभरते खतरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत ने स्थानीय और क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए आसियान देशों में आतंकवाद-रोधी केंद्रों और प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना का समर्थन किया है।
आसियान देश भारत की जलवायु-अनुकूल वैश्विक पहलों जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, आपदा प्रतिरोधक अवसंरचना के लिए गठबंधन तथा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रस्ताव में भी भाग लेते हैं।
3. भारत-आसियान आर्थिक सहयोग
भारत की आसियान पॉलिसी प्रधानमंत्री मोदी के ‘सबका साथ सबका विश्वास’ (एव्रीबाडी टुगेदर एव्रीबाडी ट्रस्ट) पर विश्वास करती है। भारत ने 2019 में व्यापार घाटे, सुरक्षा उपायों की कमी और घरेलू उद्योगों को संभावित नुकसान की चिंताओं का हवाला देते हुए क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी ) से बाहर निकलने का विकल्प चुना।
अक्टूबर 2003 में हस्ताक्षर हुए व्यापक आर्थिक सहयोग पर रूपरेखा करार के परिणामस्वरूप आसियान-भारतीय मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण हुआ जिसमें 2009 में हस्ताक्षरित वस्तुओं के व्यापार पर, 2014 में सेवाओं में व्यापार पर और 2014 में निवेश पर समझौता शामिल है। भारत-आसियान व्यापार 2023 में 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। भारत से एफडीआई 2022 में 2.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 में 5.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। आसियान-इंडिया बिज़नस काउंसिल (एआईबीसी) को फिर से सक्रिय करके निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं।
आसियान और भारत के बीच कनेक्टिविटी में सहयोग को मजबूत करने के लिए, 2024 भारत- आसियान शिखर सम्मेलन ने आसियान कनेक्टिविटी पर आसियान मास्टर प्लान (एमपीएसी) 2025/ आसियान कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजिक प्लान (एसीएसपी) और एक्ट ईस्ट पॉलिसी और एसएजीएआर के तहत क्षेत्र में भारत की कनेक्टिविटी पहलों के बीच तालमेल लाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। ये पहल इंडो-पैसिफिक में बेहतर व्यवसाय और व्यापार के लिए सुगम संपर्क सुनिश्चित करेंगी।
दोनों पक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ब्लॉकचेन तकनीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग सहित उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग कर रहे हैं और डिजिटल कनेक्टिविटी और वित्तीय प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर देते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण और उसे मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने भारत-आसियान फंड फॉर डिजिटल फ्यूचर का शुभारंभ किया, जिसमें इन क्षेत्रों में संयुक्त गतिविधियों की फंडिंग और समर्थन देना शामिल है।
ऊर्जा क्षेत्र में, ऊर्जा सहयोग के लिए आसियान कार्य योजना 2021-2025 भारत की अक्षय ऊर्जा प्राथमिकताओं के अनुरूप है और इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में वृद्धि होगी।
आगे का रास्ता
अब मैं उन चरणों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उठाए जा सकते हैं।
i. राजनीतिक सहयोग पर:
क) दोनों पक्षों को नई भारत-आसियान कार्य योजना (2026-2030) तैयार करने पर ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्य योजना अगले पांच वर्षों में भारत-आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पूरी क्षमता को साकार करने में दोनों पक्षों का मार्गदर्शन करेगी।
ख) व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देना, विशेष रूप से आसियान आउटलुक ऑन इंडो-पैसिफिक (एओआईपी) में पहचाने गए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, आसियान के नेतृत्व वाले तंत्रों के साथ और अधिक काम करने की आवश्यकता है। विशिष्ट क्षेत्रों/परियोजनाओं की पहचान की जानी चाहिए।
ग) विस्तृत और सतत क्षेत्रीय विकास के लिए भारत की इंडो-पैसिफिक पहल (आईपीओआई) और आसियान की एओआईपी को तालमेलपूर्वक आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
घ) दोनों पक्षों को 2021 में अपनाए गए क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए इंडो-पैसिफिक पर आसियान दृष्टिकोण पर सहयोग पर भारत-आसियान संयुक्त वक्तव्य के साथ-साथ 2023 के समुद्री सहयोग पर भारत-आसियान संयुक्त वक्तव्य के कार्यान्वयन को मूर्त रूप देने के लिए भी प्रयास करने होंगे।
(ii)सुरक्षा सहयोग पर:
क) भारत और आसियान संगठित अपराध से निपटने, समुद्री डकैती से निपटने और समुद्री क्षेत्र जागरूकता में क्षमता निर्माण एवं सहयोग के माध्यम से समुद्र में अच्छी व्यवस्था बनाए रखने पर अधिक ध्यान देने के साथ अपनी इंडो-पैसिफिक रणनीति को मजबूत कर सकते हैं।
(iii) आर्थिक सहयोग पर:
क) भारत को आसियान के पक्ष में बढ़ते व्यापार घाटे पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जो 2017 में 7 प्रतिशत के व्यापार घाटे से बढ़कर 2023 में 44 प्रतिशत हो जाएगा।
ख) आसियान और भारत के आपसी विकास को बढ़ावा देने के लिए, आईओआरए, बिम्सटेक और एमजीसी जैसे क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय ढांचे के भीतर तालमेल बनाना महत्वपूर्ण है।
ग) सहयोग के अन्य संभावित क्षेत्रों में भारत द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया-भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप संपर्क बनाने के लिए चेन्नई-व्लादिवोस्तोक शिपिंग कॉरिडोर और इंडिया-मिडिल ईस्ट इकनोमिक कॉरिडोर में शामिल होने के लिए आसियान देशों को आमंत्रित करना शामिल है।
घ) भारत मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ अपने सेमीकंडक्टर सहयोग का विस्तार कर सकता है, जो अमेरिका-चीन सेमीकंडक्टर प्रतिद्वंदी के रूप में सेमीकंडक्टर बाजार में अपनी पहचान बना रहे हैं।
ड़) आसियान देश भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्थापित पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र में भाग ले सकते हैं।
निष्कर्ष के तौर पर, एक्ट ईस्ट नीति के शुरू होने के बाद से पिछले दस वर्षों में, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और आसियान के साथ हमारे संबंधों में पूर्ण स्पेक्ट्रम वृद्धि हुई है। हम दोनों पक्षों में एक दूसरे की सुरक्षा समस्याओं और विकास की महत्वाकांक्षा के प्रति बढ़ी हुई प्रशंसा और समझ के साथ-साथ सहयोग करने की बढ़ी हुई इच्छा भी देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ प्राचीन और मध्यकालीन काल के भारत के ऐतिहासिक संबंधों में दोनों पक्षों की रुचि और प्रशंसा में पुनरुत्थान हुआ है, जो मजबूत सांस्कृतिक आत्मीयता के निर्माण का आधार प्रदान करता है, और पुरातात्विक संरक्षण में संबंधों का भी आधार है। इन देशों विशेष रूप से मलेशिया और सिंगापुर में भारतीय प्रवासियों का कल्याण, भारतीय मूल के लोगों का उनके नागरिकता वाले देशों में पूर्ण सम्मिलन, भारत के लिए महत्वपूर्ण रुचि का विषय है और सरकार को समय-समय पर इन देशों के साथ इस मुद्दे को उठाने में सक्रिय होने की आवश्यकता है। शिक्षा सहित सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, डार्क शिपिंग, माल और हथियारों की तस्करी और घोटाले केंद्रों से लड़ने के लिए सहयोग करने के प्रयास करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्षेत्र में भारत की विकास साझेदारी पहल सराहनीय है और इसे क्षेत्र के देशों की आवश्यकताओं और आपसी क्षमताओं के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सहयोग का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विकास की व्यापक संभावना है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति को ग्लोबल साउथ के अपने दृष्टिकोण के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए। भारत वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट पहल में क्षेत्र के नेताओं की भागीदारी की सराहना करता है। संक्षेप में, हमारे संबंधों को और आगे ले जाने के लिए एक पूर्ण एजेंडा है।
मुझे यकीन है कि इस सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं से कई उपयोगी अवलोकन और सुझाव सामने आएंगे। मुझे उम्मीद है कि छात्र इन चर्चाओं में सक्रिय रूप से योगदान देंगे। मैं सभी वक्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी और सी3एस के साथ निरंतर सहयोग की आशा करता हूं।
*****