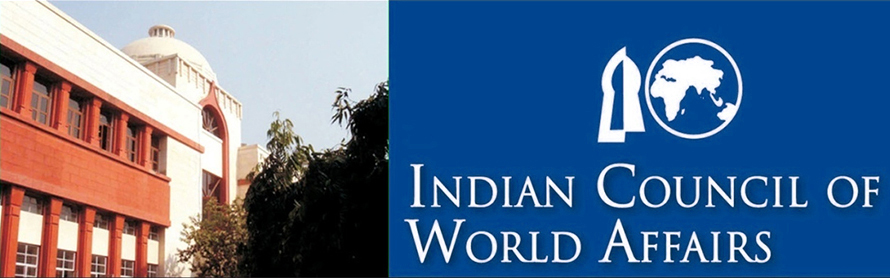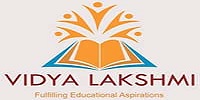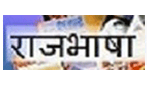भारतीय वैश्विक परिषद
सप्रू हाउस, नई दिल्ली'1994 के मास्को घोषणापत्र के तीस वर्ष : बदलती दुनिया में बहुलवादी राज्य'
8 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन और रूस, यूक्रेन और बेलारूस के बीच बेलोवेज़्स्काया समझौते पर हस्ताक्षर ने वैश्विक राजनीति में एक गहन बदलाव को चिह्नित किया। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा, जिसका श्रेय उसकी रक्षा, वित्तीय प्रणालियों, आर्थिक मजबूती और सुरक्षा उपायों में स्थायी क्षमताओं को जाता है। इसने भारत और रूस के लिए भी महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश कीं, जिसके लिए दोनों को स्पष्ट रूप से बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल ढलना आवश्यक था।
भारत के लिए, सोवियत संघ, जो एक करीबी और भरोसेमंद दोस्त था, के साथ एक सहज संबंध समाप्त हो गया। भुगतान संतुलन के एक बड़े संकट का सामना करते हुए, इसने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की परिकल्पना करते हुए आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसने इसके बाद के दीर्घकालिक विकास की नींव रखी, जबकि अपनी विदेश नीति को पुनः उन्मुख और विविधतापूर्ण बनाकर अधिक रणनीतिक स्वायत्तता की मांग की।
इस बीच, रूस ने केन्द्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था से बाजार की शक्तियों द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित होने की महत्वपूर्ण चुनौती का सामना किया, और साथ ही वैश्विक मामलों में अपनी भूमिका को पुनः स्थापित और पुनर्परिभाषित किया। सोवियत संघ के एकमात्र अनुचर राज्य के रूप में, रूस को व्यापक राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंध विरासत में मिले, लेकिन उसे आर्थिक उथल-पुथल और घरेलू संघर्षों के साथ-साथ वैश्विक प्रभाव में भी कमी का सामना करना पड़ा। भ्रष्टाचार, अत्यधिक मुद्रास्फीति और बढ़ती असमानता ने इसके "शॉक थेरेपी" सुधारों में जनता के विश्वास को कमजोर कर दिया। इस स्थिति में महत्वपूर्ण आंतरिक संघर्षों के प्रबंधन की आवश्यकता थी, जिसमें अक्टूबर 1993 में राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन और रूसी संसद के बीच टकराव, तथा चेचन्या की स्वतंत्रता का दावा, तथा सोवियत संघ के बाद के क्षेत्र में रूसी प्रभाव के लिए उत्पन्न चुनौतियां शामिल थीं। इसी समय, विदेश मंत्री आंद्रेई कोज़ीरेव के नेतृत्व में रूसी विदेश नीति ने शुरू में लगभग विशेष रूप से पश्चिम के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दी और प्रमुखता दी।
1994 मास्को घोषणा : मुख्य विशेषताएं
परिणामस्वरूप, 1993 में एक नई मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर होने तक भारत और रूस के बीच संबंध कमजोर हो गए। द्विपक्षीय चर्चाओं का पुनरुद्धार अगले वर्ष प्रधान मंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव की रूस यात्रा के साथ हुआ, जहां 30 जून 1994 को प्रधान मंत्री राव और राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन द्वारा बहुलवादी राज्यों के हितों पर मास्को घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। घोषणापत्र में शीत युद्ध के बाद की नई वैश्विक स्थिति में भारत और रूस द्वारा अपनी स्थिति की रणनीतिक सराहना प्रतिबिंबित हुई, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तीस वर्ष पहले थी। इस दस्तावेज़ में भारत और रूस के आपसी हितों और सामूहिक मुद्दों को रेखांकित किया गया है, जो दोनों ही सबसे बड़े, बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक लोकतंत्रों में से हैं। यूगोस्लाविया के विघटन और उस अवधि के दौरान वैश्विक स्तर पर देखी गई बढ़ती केन्द्रापसारक शक्तियों के आलोक में, इसने शीत युद्ध के बाद के संदर्भ में बड़े, बहुलवादी, लोकतांत्रिक राष्ट्रों के सामने आने वाली आम चुनौतियों पर भी जोर दिया, और इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। घोषणापत्र में अन्य राज्यों या बहुपक्षीय संगठनों की भूमिका पर कोई चर्चा नहीं की गई तथा इसमें ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए ठोस समयसीमा निर्दिष्ट करने से भी परहेज किया गया, क्योंकि इसमें एक दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया।
क . भारत एवं रूस की सामान्य विशेषताएँ
बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक राष्ट्रों के रूप में भारत और रूस की समान विशेषताएं 1994 के मास्को घोषणापत्र का आधार रही हैं। अपने-अपने बहुलवादी और लोकतांत्रिक समाजों की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को साझा, दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में इसमें प्रस्तुत किया गया था। घोषणापत्र में भारत के लिए अपने विदेशी संबंधों के संचालन में रणनीतिक स्वायत्तता के पसंदीदा मार्ग को रेखांकित किया गया, न कि उभरती भू-राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए पश्चिम पर अत्यधिक निर्भरता की ओर झुकाव को। इसने इस बात के महत्व को भी रेखांकित किया कि अपने कम होते वैश्विक प्रभाव के दौर में रूस को न केवल पश्चिम की ओर देखने तक सीमित रहना चाहिए, बल्कि भारत जैसे दीर्घकालिक और विश्वसनीय साझेदार के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को फिर से मजबूत करना चाहिए। घोषणापत्र में वैचारिक बारीकियों को छोड़ दिया गया तथा भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया गया, तथा शीत युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के एकध्रुवीय प्रभाव से परिभाषित युग के दौरान वैश्विक मामलों पर अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया गया।
ख. बहुलवाद की रक्षा करना
घोषणापत्र में पारस्परिक लाभ देने वाले सहकारी प्रयासों के लिए वैचारिक और विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों को स्वीकार किया गया। इसमें विशेष रूप से बहुलवादी राज्यों की एकता के लिए नई चुनौतियों के उभरने, विशेष रूप से आक्रामक राष्ट्रवाद, धार्मिक और राजनीतिक उग्रवाद, आतंकवाद और अलगाववाद से बढ़ते खतरों का उल्लेख किया गया, जो इन राज्यों की एकजुटता को कमजोर करते हैं।
ग. लोकतांत्रिक समाज के मार्गदर्शक सिद्धांत
घोषणापत्र के अनुसार, भारत और रूस सबसे बड़े बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक राष्ट्रों में से हैं, तथा उन्होंने लोकतंत्र के लिए खतरों का विरोध करने में दूसरों के साथ-साथ अपनी विशेष जिम्मेदारी को पहचाना। उन्होंने समानता, कानून का शासन, मानवाधिकारों का पालन, पसंद की स्वतंत्रता और सहिष्णुता जैसे हर लोकतांत्रिक समाज में अंतर्निहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रति अपने पालन की पुष्टि की। उन्होंने अपने इस विश्वास पर बल दिया कि ऐसे सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी समान रूप से लागू होते हैं, तथा इस संदर्भ में ‘राज्यों की संप्रभुता, समानता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व’ की वकालत की।
घ. आत्मनिर्णय
घोषणापत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत और रूस के लोगों ने अपने आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रयोग करके वैध रूप से संप्रभु और स्वतंत्र राज्यों का गठन किया है, जहाँ लोगों की इच्छा प्रतिनिधि लोकतंत्र में उनकी भागीदारी के माध्यम से परिलक्षित होती है। इस प्रकाश में, इसने आत्मनिर्णय के स्थापित सिद्धांतों को कमजोर करने के उद्देश्य से किसी भी पहल के प्रति सावधानी से आगाह किया।
ङ. धार्मिक एवं जातीय विविधता
घोषणापत्र में भारत और रूस में कई धर्मों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को मान्यता दी गई है, तथा धार्मिक बहिष्कार और उग्रवाद के किसी भी रूप को दृढ़ता से खारिज किया गया है। इसने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक आश्वासनों को रेखांकित किया है, जो दोनों देशों में बरकरार हैं, तथा इन गारंटियों को उनके दैनिक जीवन के लिए मौलिक बताया है। इस आलोक में, पार्टियों ने अपने समुदायों की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता की रक्षा करने का संकल्प व्यक्त किया, साथ ही अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक नफरत को भड़काने या आक्रामक राष्ट्रवाद और धार्मिक कट्टरता की वकालत करने को असहनीय घोषित किया।
भारत और रूस ने घोषणापत्र में ‘जातीय या धार्मिक समूहों के बीच संबंधों में अस्थिरता, उन्हें जबरन विस्थापित करने के प्रयास, जातीय सफाया और निहित स्वार्थों से प्रेरित आंतरिक और सीमापार आतंकवाद को बढ़ावा देने’ की अस्वीकार्यता के बारे में अपने विश्वास की भी पुष्टि की।
च. क्षेत्रीय अखंडता की पुष्टि
अपने इस विश्वास पर बल देते हुए कि बड़े बहुजातीय राज्य करोड़ों लोगों के भाग्य के लिए "विशेष जिम्मेदारी" वहन करते हैं, भारत और रूस ने घोषणापत्र में बहुजातीय राज्यों की व्यवहार्यता के एक प्रमुख कारक के रूप में राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और एकता के सम्मान के सिद्धांत के बिना शर्त पालन की वकालत की है। उल्लेखनीय रूप से, उन्होंने एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपना समर्थन दोहराया है, “जैसा कि कानून द्वारा गठित और उनके संबंधित संविधानों में निहित है।” इस बात पर जोर देते हुए कि बहुजातीय और बहुधार्मिक राज्यों के सफल विकास ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा दिया है, भारत और रूस ने अन्य देशों से भी ऐसे राज्यों की अखंडता का सम्मान करने का आग्रह किया।
छ. अन्य पहचानी गई चिंताएँ
यह ध्यान देने योग्य है कि भारत ने घोषणापत्र में पूर्व सोवियत संघ में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए समान कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में रूस की चिंताओं को मान्यता दी, और जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक समाजों में गारंटीकृत उनके मौलिक मानवाधिकारों को संरक्षित किया जाना चाहिए। बदले में, रूस ने सामाजिक एकता को बढ़ावा देने, विकास को आगे बढ़ाने और अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को महत्व दिया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में संचलन
इस पर व्यापक वैश्विक ध्यान आकर्षित करने की मांग करते हुए, भारत और रूस ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधियों के माध्यम से संयुक्त रूप से 15 जुलाई 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव को मास्को घोषणा पत्र प्रेषित किया, और अनुरोध किया कि इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के दस्तावेज़ के रूप में प्रसारित किया जाए।
समकालीन प्रासंगिकता
तीस साल बाद भी, मास्को घोषणापत्र में व्यक्त सिद्धांत काफी प्रासंगिक बने हुए हैं। वैश्विक अनिश्चितता के दौर में बहुलवादी समाजों की सुरक्षा के लिए भारत और रूस दोनों के लिए प्रस्तुत दृष्टिकोण ने उनके द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया है। एकतरफावाद का विरोध करते हुए घोषणापत्र में आतंकवाद, अलगाववाद और बाहरी हस्तक्षेप जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया - ये चिंताएं न केवल समकालीन भूराजनीति में गूंजती रहती हैं, बल्कि समय के साथ इनका परिमाण भी बढ़ता गया है।
1994 के मास्को घोषणापत्र का समर्थन भारत-रूस संबंधों को सहारा देने वाली मजबूत नींव का उदाहरण है, यहां तक कि भू-राजनीतिक मतभेदों से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भी। घोषणापत्र में व्यक्त सिद्धांत हमारे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक प्रभाव के रूप में काम करना जारी रखते हैं। पूरी तरह से गैर-वैचारिक भाषा में तैयार किए गए घोषणापत्र के कई प्रावधान आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे तीन दशक पहले उनके समझौते के समय थे।
रणनीतिक साझेदारी की ओर एक कदम
अक्टूबर 2000 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की पहली यात्रा के अंत में जारी संयुक्त वक्तव्य में 1994 के मास्को घोषणापत्र का संदर्भ दिया गया था, जिसमें भारत और रूस ने कानून द्वारा परिभाषित और अपने-अपने संविधानों में निहित एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी। इस विशेष उल्लेख ने बहुलवादी समाजों के लिए खतरों से निपटने के लिए उनके सामूहिक समर्पण के अलावा, क्षेत्रीय अखंडता के लिए दोनों देशों द्वारा आपसी समर्थन पर दिए जाने वाले निरंतर महत्व को उजागर किया।
1994 में मास्को घोषणापत्र ने भारत और रूस के बीच सामरिक साझेदारी के विकास के लिए मंच तैयार किया, एक अवधारणा जिस पर 1998 में सहमति हुई और 1998 के अंत में प्रधान मंत्री येवगेनी प्रिमाकोव की भारत यात्रा के दौरान इस पर बल दिया गया। 2000 में भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन द्वारा सामरिक साझेदारी पर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ यह साझेदारी और भी मजबूत हुई और बाद में 2010 में राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान इसे विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी में विस्तारित किया गया।
बहुलवाद, आपसी सम्मान और साझा रणनीतिक हितों के सिद्धांतों पर आधारित, बहुलवादी राज्यों के हितों पर 1994 के मास्को घोषणापत्र में स्थापित सिद्धांत भारत और रूस के लिए काफी प्रासंगिक हैं। चूंकि दोनों देश बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य की जटिलताओं से निपट रहे हैं, इसलिए ये सिद्धांत उनके स्थायी राष्ट्रीय हितों को दर्शाते हैं।
*****
*राजदूत अजय मल्होत्रा रूस में भारत के पूर्व राजदूत हैं। वे रोमानिया, अल्बानिया, मोल्दोवा और कुवैत में भी भारत के राजदूत रह चुके हैं।