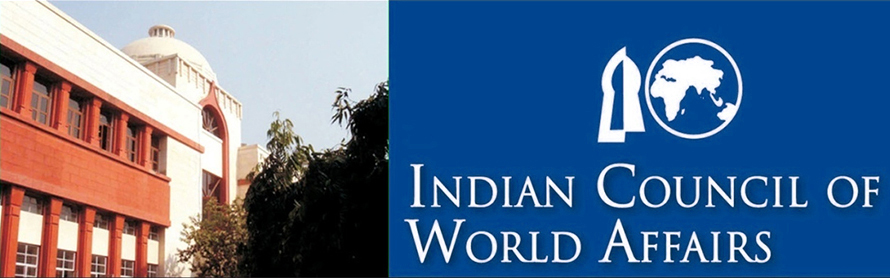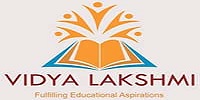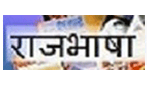भारतीय वैश्विक परिषद
सप्रू हाउस, नई दिल्ली'बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में भारत की विदेश नीति' पर राष्ट्रीय सेमिनार में आईसीडब्ल्यूए के पूर्व महानिदेशक राजदूत राजीव भाटिया की टिप्पणियाँ, आइजोल, 25 नवंबर 2024
'बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में भारत की विदेश नीति' आईसीडब्ल्यूए-मिजोरम विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेमिनार में आईसीडब्ल्यूए के पूर्व महानिदेशक अंब राजीव भाटिया की टिप्पणियाँ, आइजोल, 25 नवंबर 2024
मंच पर प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति, सम्मानित अतिथि, संकाय सदस्य और प्रिय छात्र,
इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेना और इसके उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में बोलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह आयोजन स्थल, मिजोरम, उत्तर-पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जिसका अद्वितीय महत्व है। चुना गया विषय उपयुक्त और समयानुकूल है। अब, यह हम पर, प्रतिभागियों पर, अपने विविध लेकिन विचारशील दृष्टिकोण प्रस्तुत करके कार्यक्रम की सफलता में योगदान करने का दायित्व है।
मैं इस भव्य निमंत्रण के लिए मिजोरम विश्वविद्यालय और आईसीडब्ल्यूए को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिसके महानिदेशक के रूप में तीन वर्षों तक नेतृत्व करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ।
चूंकि मैं उद्घाटन सत्र में बोल रहा हूं, इसलिए क्या मैं चुने गए विषय के कई पहलुओं को कवर करने की स्वतंत्रता ले सकता हूं? हालांकि, मैं समय की कमी से पूरी तरह वाकिफ हूं। नतीजतन, मैं भारत की विदेश नीति के केवल चुनिंदा पहलुओं को संबोधित करने का इरादा रखता हूं, जिसमें इसके मूलभूत दर्शन, ऐतिहासिक विकास और समकालीन स्थिति शामिल हैं, जिसमें दक्षिण एशिया, पूर्वी क्षेत्र, अफ्रीका और इसके बहुपक्षीय राजनयिक प्रयासों में देश की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है।
दर्शन और विकास
36 वर्षों के अनुभव वाले राजनयिक और 22 वर्षों से विदेश नीति के छात्र के रूप में, मैं इस बात से गहराई से अवगत हूँ कि विदेश नीति राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। सभी राष्ट्र समान उद्देश्यों को प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं: अपनी क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करके सुरक्षा सुनिश्चित करना; जलवायु परिवर्तन संबंधी विचारों, तकनीकी प्रगति और अन्य आर्थिक परिवर्तनों के साथ संरेखित सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना; और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए राष्ट्रीय गरिमा को बनाए रखना। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत ने सदैव एक प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य राष्ट्रों के हितों, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कल्याण और विश्व शांति को भी ध्यान में रखा गया है।
भारत की विदेश नीति का दर्शन इसकी प्राचीन सभ्यतागत विरासत और विश्व को एक बड़े परिवार के रूप में मानने की मान्यता, चाणक्य जैसे विद्वानों के लेखन तथा देश के लंबे स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव और आदर्शों द्वारा आकार लेता है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने कई पीढ़ियों तक हमारी विदेश नीति की धारणाओं को आकार दिया। विशेष रूप से, 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से पिछले 77 वर्षों में, नीति में देश, क्षेत्र और दुनिया में बड़े पैमाने पर परिवर्तनों के अनुरूप कई बदलाव हुए हैं। साथ ही, नीति की नींव और अन्य परिभाषित विशेषताओं को बोधगम्य निरंतरता के साथ प्रभावित किया गया है।
हमारी विदेश नीति के विकास की कहानी को विच्छेदित करने के कई तरीके हैं। यही कारण है कि मैं संगोष्ठी के अवधारणा नोट से असहमत हूं, जो पिछले सात दशकों को केवल तीन अवधियों में विभाजित करता है। मेरा सुविचारित विचार यह है कि इस विकास का छह अलग-अलग चरणों में बेहतर मूल्यांकन किया जा सकता है: i) नेहरू वर्ष (1947-64), ii) नेहरू के बाद के वर्ष, iii) गठबंधन युग (1991-99), iv) अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में, v) डॉ मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में, और vi) नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में।
मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री और पीएमओ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री के साथ मिलकर देश की विदेश नीति तैयार करने और कूटनीति चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
मेरा यह भी मानना है कि 1947 से 2024 के बीच हमारे चौदह प्रधानमंत्रियों में से तीन “विदेश नीति प्रधानमंत्री” के रूप में उभर कर सामने आते हैं, और वे हैं: नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेन्द्र मोदी।
संदर्भ और विषय-वस्तु
यह एक सत्य है कि विदेश नीति की व्यापक विषय-वस्तु समय के साथ-साथ राष्ट्र-राज्य और उसके आसपास की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के साथ बदलती रहती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय बाद ही भारत को बाहरी खतरों और घुसपैठ से स्वयं को सुरक्षित रखने की आवश्यकता, एशिया और अफ्रीका के अन्य भागों में स्वतंत्रता आन्दोलनों को तीव्र करने का संकल्प, तथा गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और मजबूत संस्थाओं की स्थापना को प्राथमिकता देने की अनिवार्यता ने प्रेरित किया।
सात दशक बाद, हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं अलग हैं। हम विकास, त्वरित आर्थिक विकास और सतत विकास को सुरक्षित करने के लिए एआई सहित आधुनिक तकनीकों के उपयोग के व्यापक उद्देश्य के लिए विदेश नीति और कूटनीति को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज का ध्यान वैश्विक दक्षिण की एकजुटता को मजबूत करने और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुरक्षित करने पर है। भारत सरकार द्वारा 2022-23 के दौरान जी20 की अध्यक्षता के दौरान इन और अन्य लक्ष्यों को तीखे और प्रेरक ढंग से प्रस्तुत किया गया। फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा कभी भी मुख्य प्राथमिकताओं से दूर नहीं रही है। इसलिए, आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में तेज़ी लाकर अपनी सीमाओं की रक्षा करना और पाकिस्तान और चीन जैसे दो मुश्किल पड़ोसियों से निपटने के लिए सभी ज़रूरी उपाय करना, हमेशा हमारे नीति निर्माताओं का सबसे ज़्यादा ध्यान रहा है।
विदेश नीति का अध्ययन और मूल्यांकन उसके समय के संदर्भ में किया जाना चाहिए। आज भारत के लिए विशेष रूप से वैश्विक और क्षेत्रीय संदर्भ क्या है?
पहला, यह ‘बहु-संकट’ का युग है जो 2020 में कोविड महामारी के प्रकोप के साथ शुरू हुआ और इसके बाद यूरोप और मध्य पूर्व में विनाशकारी युद्ध हुए, जबकि अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता गहरी हुई, विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में।
दूसरा, यह पुनर्संतुलन का समय है, जब आर्थिक शक्ति और अन्य प्रकार की शक्तियां अटलांटिक से प्रशांत की ओर, तथा अमेरिका और यूरोप से एशिया की ओर स्थानांतरित हो रही हैं, क्योंकि चीन, भारत और अन्य राष्ट्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
तीसरा, बहुध्रुवीयता का उदय अंतरराष्ट्रीय जीवन का एक तथ्य है, जहां सत्ता के लगभग एक दर्जन ध्रुव घटनाओं, प्रवृत्तियों और आख्यानों के पैटर्न को आकार देते हैं। किसी भी तरह से वे समान नहीं हैं। इसके अलावा, इस बहुध्रुवीयता के नीचे पश्चिम (यानी, जी 7 और नाटो) और पूर्व (यानी, चीन और रूस) के बीच विभाजन के इर्द-गिर्द निर्मित द्विध्रुवीयता का एक सीमित रूप निहित है।
चौथा, बहु-संरेखण और रणनीतिक स्वायत्तता में भारत का विश्वास एक पश्चिमी समर्थक नीति अभिविन्यास के साथ मिश्रित है जो अभी भी उसे रूस के साथ अपने विरासत संबंधों को बरकरार रखने और गहरा करने और चीन के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को प्रबंधित करने की अनुमति देता है। अब, वैश्विक दक्षिण से संबंधित इसकी नेतृत्व महत्वाकांक्षाएं इसे एक संतुलित मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे भारत को पश्चिम और पूर्व तथा उत्तर और दक्षिण के बीच एक सेतु के रूप में काम करने में मदद मिलती है। 2024 के क्वाड और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर, नई दिल्ली ने खुद को एक उल्लेखनीय भू-राजनीतिक स्थिति में स्थापित किया। हालाँकि, इस लाभकारी भूमिका में अंतर्निहित जोखिम और कमजोरियाँ हैं।
पांचवां, समकालीन जरूरतों और रुझानों के साथ विदेश नीति का एजेंडा अधिक विविधतापूर्ण और जटिल हो गया है। वर्तमान में, जब भारत के विदेश मंत्री एशिया, यूरोप या अन्य जगहों पर अपने समकक्षों के साथ बातचीत करते हैं, तो वे हमेशा महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, जलवायु लक्ष्यों और जलवायु वित्त, कट्टरपंथ और आतंकवाद से संबंधित वित्तपोषण पर अंकुश लगाने, महत्वपूर्ण खनिजों, ऋण बोझ, गतिशीलता और प्रवासन के बारे में बात करते हैं। भारत के पहले विदेश मंत्री को ऐसे अधिकांश मामलों से निपटना नहीं पड़ा।
पहलुओं का चयन करें
भारत की विदेश नीति के लिए प्राथमिकताओं की सूची लंबी है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन इसे तैयार कर रहा है। समय की कमी के कारण, मैं यहां केवल चार विशिष्ट मुद्दों की ओर ध्यान आकषत करना चाहूंगा।
दक्षिण एशिया, हमारा निकटतम पड़ोस, इस क्षेत्र के प्रति हमारे दृष्टिकोण और विश्व में हमारी भूमिका और स्थान को आकार देना जारी रखेगा। इस दशक में, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश और म्यांमार और नेपाल से लेकर श्रीलंका और मालदीव तक हमारे पड़ोसियों के संबंध में विकास ने हमारी महान शक्ति महत्वाकांक्षाओं और स्थिरता, सुरक्षा और प्रगति लाने की हमारी क्षमता के लिए इस क्षेत्र की निरंतर और महत्वपूर्ण प्रासंगिकता को प्रदर्शित किया है। हमें ‘पड़ोसी पहले’ नीति की प्रभावशीलता, आज हम अपने सभी पड़ोसी देशों के मुकाबले किस तरह खड़े हैं, तथा क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण के प्रति दृष्टिकोण पर स्पष्ट बहस की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को देखते हुए कि यह सेमिनार मिजोरम की राजधानी आइजोल में हो रहा है, भारत की म्यांमार नीति और भारत-म्यांमार संबंधों पर केंद्रित चर्चा पर भी विचार किया जाना चाहिए।
भारत के पूर्वी क्षेत्र के साथ संबंध, या जैसा कि अवधारणा पत्र में कहा गया है, विदेश नीति का 'पूर्वी अभिविन्यास' भी काफी महत्वपूर्ण है। 1955 का बांडुंग सम्मेलन इसी क्षेत्र में आयोजित किया गया था। यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अग्रदूत था जिसने लगभग 40 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार दिया। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से, हम ‘लुक ईस्ट’ और ‘एक्ट ईस्ट’ नीतियों के चरणों से गुज़रे हैं। अब हम इंडो-पैसिफिक रणनीति या नीति के नवीनतम चरण में हैं, जिसमें इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (आईपीओआई) और क्वाड जैसी विशेष परियोजनाओं पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया गया है। दोनों का ‘चीन कारक’ से बहुत कुछ लेना-देना है, भले ही आधिकारिक कथन इसके विपरीत हों। यहाँ हमारी बहस से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि क्या इन नीतिगत पहलों को लागू करना अब तक इष्टतम रहा है और डोनाल्ड ट्रम्प के व्हाइट हाउस में वापस आने से इनका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है।
अफ्रीका और ग्लोबल साउथ भारत की प्राथमिकताओं में एक विशेष स्थान रखते हैं। पूर्व-कोविड अवधि के दौरान, मोदी सरकार ने अफ्रीका के साथ बहुआयामी साझेदारी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जिसे आधिकारिक तौर पर 'ग्लोबल साउथ के मूल' के रूप में दर्शाया गया है। फिर, बाहरी कारकों के कारण गति धीमी हो गई। अब, भारत के नेतृत्व और भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा चार अफ्रीकी देशों - अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी और नाइजीरिया की हालिया यात्राओं के कारण अफ्रीकी संघ के जी-20 में स्थायी सदस्य के रूप में प्रवेश के साथ उत्साह में एक नई तेजी देखी गई है। अफ्रीका में कोविड के बाद के परिदृश्य का गहन विश्लेषण चुनौतियों और अवसरों दोनों को उजागर करता है, तथा नई दिल्ली के लिए अपने रणनीतिक ढांचे को तदनुसार समायोजित करने के महत्व को रेखांकित करता है।
अंत में, भारत की बहुपक्षीय कूटनीति को वस्तुनिष्ठ परीक्षण और मूल्यांकन की आवश्यकता है। शायद भारत के लिए छह सबसे महत्वपूर्ण बहुपक्षीय समूह जी20, क्वाड, जी7 (जहां भारत को लगभग स्थायी अतिथि का दर्जा प्राप्त है), ब्रिक्स, बिम्सटेक और एससीओ हैं। आदर्श रूप से, प्रत्येक को एक अलग सत्र और विशेषज्ञों के एक अलग समूह की आवश्यकता होती है। शायद भविष्य में इस विषय पर एक विस्तृत संवाद आयोजित किया जा सकता है।
निष्कर्ष
मैं दो अतिरिक्त बातें कहना चाहता हूं।
सबसे पहले, अपनी नवीनतम पुस्तक में प्रोफेसर श्रीराम चौलिया ने भारत के अपने सात निकटतम रणनीतिक साझेदारों - अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, यूएई, फ्रांस और रूस के साथ संबंधों का विश्लेषण किया है। हाल ही में दिल्ली में इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रों के बीच मित्रता का संबंध “समान हितों” के साथ-साथ “प्रवृत्ति, विश्वास, एकजुटता और सम्मान” से भी है। उन्होंने कहा कि मित्रता "अनन्य भी नहीं है।" मेरा सुझाव है कि यह भारत के लिए एक प्रतिबंधात्मक सूची है, जो भविष्य में एक अग्रणी शक्ति बनने की आकांक्षा रखता है और एक संतुलनकारी शक्ति होने से संतुष्ट नहीं है। इसलिए, इंडोनेशिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और अर्जेंटीना जैसे वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करके इस सूची का विस्तार करने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।
अंतिम विचार के रूप में, मैं आप सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति के महत्व पर प्रकाश डालना चाहूँगा, प्रिय छात्रों। आपका अध्ययन का क्षेत्र चाहे जो भी हो - चाहे वह विज्ञान, आईटी, वाणिज्य, व्यवसाय प्रबंधन या मानविकी हो - अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का आपके जीवन और करियर पथ पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, आपके लिए इस सेमिनार में पूरी तरह से शामिल होना समझदारी है। मैं इस सेमिनार में आपकी सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ।
*****